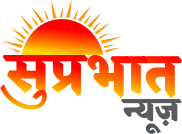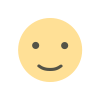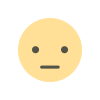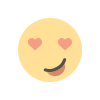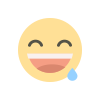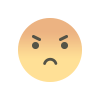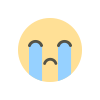नकली कीटनाशक बने किसानों की आय बढ़ाने की राह में रोड़ा
नकली कीटनाशकों का कारोबार तकरीबन 50 अरब रुपये तक पहुंच चुका है।

नयी दिल्ली : देश के लगभग 150 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने में नकली कीटनाशक सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभर रहे हैं।
एक अनुमान के अनुसार देश में नकली कीटनाशकों का कारोबार तकरीबन 50 अरब रुपये तक पहुंच चुका है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कीटनाशकों का कारोबार 229.4 अरब डॉलर है और वर्ष 2028 तक 342.3 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। कीटनाशक क्षेत्र की वृद्धि दर 6.6 रहने का अनुमान लगाया गया है।
इन कीटनाशकों में ऐसे तत्वों और रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य कारणों से भारत में प्रतिबंधित है। कृषि बाजार में नकली कीटनाशकों की बिक्री से न केवल सरकार को राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है, बल्कि किसानों की फसलें भी खराब हो रही हैं। पिछले साल राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान की सीमा के साथ सटे इलाकों में टिड्डी दल के हमलों से फसलों को नहीं बचा पाने में नकली कीटनाशकों की प्रमुख भूमिका रही। टिड्डी दल के हमलों से फसलों को बचाने में किसानों ने जिन कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, वे गुणवत्तापूर्ण नहीं थे। इससे किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ा। कीटनाशक खरीदने के लिए किसानों को धन व्यय करना पड़ा और फसल भी नहीं बचा पाए।
एक सर्वेक्षण के अनुसार बाजार में कई तरह के नकली कीटनाशक उपलब्ध हैं। पहली श्रेणी में ऐसे नकली कीटनाशक है जो नामी गिरामी कंपनियों के नाम से बनाए जाते हैं और बाजार में उन कंपनियों के नाम के साथ बेचे जाते हैं। इन कीटनाशकों की प्रभावशीलता बहुत कम है और यह किसानों को धोखा देते हैं। कीट, खरपतवार और अन्य हानिकारक तत्वों का निपटारा नहीं होता है। दूसरी श्रेणी में ऐसे कीटनाशक हैं, जो रजिस्टर्ड या पंजीकृत नहीं हैं और उन्हें बाजार में बेचने की अनुमति भी नहीं हैं। ऐसे कीटनाशकों से फसल की गुणवत्ता खराब होती है और अक्सर निर्यात में बाधा आती है। ऐसे कीटनाशकों में निर्धारित मात्रा से ज्यादा विषैले तत्व मिलाए जाते हैं, जिनका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरी श्रेणी में ऐसे कीटनाशक भारतीय बाजार में उपलब्ध है, जिनको भारत में बेचने की अनुमति नहीं है। यह कीटनाशक भारतीय बाजार में तस्करी के माध्यम से लाये जाते हैं। चूंकि ये कीटनाशक चोरी छुपे देश में लाये जाते हैं और इसी तरीके से बेचे जाते हैं तो उनके बारे में किसानों को ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। फसलों में इनका उपयोग उचित तरीके से नहीं होता है और अक्सर फसल गुणवत्तापूर्ण नहीं होती है। जिसका खामियाजा फसल के उपरांत किसानों को और उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है।
किसान संगठनों और कृषि से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि राज्य स्तर पर कीटनाशक अधिनियम 1968 को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है और इसके लिए उचित प्रणालीगत व्यवस्था भी नहीं है। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के साथ गठजोड़ और प्रभाव के कारण नकली कीटनाशक बनाने वाले संस्थान सामान्य तौर पर बच निकलते हैं। आरंभिक कार्रवाई दुकानदारों और किसानों पर हो जाती है। किसान संगठनों और कृषि कंपनियों का कहना है कि नकली कीटनाशक का उत्पादन, वितरण, बिक्री और प्रयोग रोकने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए और स्थानीय स्तर पर संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
कृषि और किसानों के कल्याण की संस्था फाऊंडेशन फार द ग्रोथ आफ न्यू इंडिया - एफजीएनआई के वरिष्ठ सलाहकार आर जी अग्रवाल ने कहा कि किसानों को गुणवत्ता युक्त और उचित कीटनाशक उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि की जा सकती है। सामान्य तौर पर किसान फल, साग सब्जी, अनाज और तिलहन - दलहन के लिए एक ही कीटनाशक का प्रयोग करता है। इससे किसान को फसल हानि होने के साथ-साथ धन का भी नुकसान होता है। उपभोक्ताओं को भी स्वास्थ्य के अनुकूल फसल उत्पाद नहीं मिल पाते हैं और निर्यात प्रभावित होता है। कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों तथा सरकार को किसानों के लिए कीटनाशकों के प्रयोग के संबंध में विशेष अभियान चलाने चाहिए। इन अभियानों में किसानों को कीटनाशकों के प्रयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। प्रत्येक फसल और उपज के लिए अलग-अलग कीटनाशक की जानकारी किसानों को देनी चाहिए। इसके अलावा फसल के विभिन्न स्तरों पर कीटनाशकों का प्रयोग निर्धारित होना चाहिए।
कृषि उत्पादों का निर्यात एक अन्य क्षेत्र है जो किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन अनेक बार भारतीय कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में केवल इसलिए प्रतिबंधित हो जाते हैं कि उनमें निर्धारित मात्रा से अधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया गया है। इस संबंध में सरकार को और कृषि कंपनियों को ध्यान देने की जरूरत है, जिससे अनुचित कीटनाशक किसानों तक नहीं पहुंचे। इसके लिए कीटनाशक अधिनियम 1968 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करना होगा।
कीटनाशकों के प्रयोग में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देकर किसानों के धन और श्रम में बचत की जा सकती है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल न केवल परंपरागत कृषि उपकरणों में किया जा सकता है, बल्कि ड्रोन आदि की प्रयोग से अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। सरकार ने हाल में ही ड्रोन संचालन के लाइसेंस प्रदान करना आरंभ किया है। किसान संगठनों और कृषि कंपनियों को किसानों को ड्रोन लाइसेंस लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ड्रोन के उचित प्रयोग से कीटनाशकों की बर्बादी भी रोकी जा सकती है और उनका अत्यधिक प्रयोग सीमित किया जा सकता है। विशेष तौर पर बागवानी और साग सब्जी की फसलों में ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कीटनाशकों का प्रयोग मृदा के प्रकार के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा स्थान विशेष की जलवायु की भी इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है। कीटनाशकों के प्रयोग को लेकर देश में बड़े स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इस विशाल और विराट लक्ष्य के लिए सरकारी निजी भागीदारी में काम किया जाना चाहिए।
श्री अग्रवाल ने कहा कि तकरीबन 15 करोड से 17 करोड़ परिवार कृषि आधारित कामकाज पर अपना जीवन यापन करते हैं। देश में कृषि में विविधता भी बहुत है, इसलिए प्रयोगशालाओं का स्थानीय स्तर पर होना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए असम में खेती के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक और कीटनाशक पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उचित नहीं होंगे। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में किये गये प्रयोग केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सफल नहीं होंगे। महाराष्ट्र और ओडिशा में भी अलग-अलग तकनीक अपनानी होगी। वास्तव में कृषि के लिए देश में एक जन आंदोलन शुरू करने की जरूरत है जिसमें सरकार, निजी कंपनियों और सामाजिक संस्थाओं को एक साथ जुड़ना होगा।