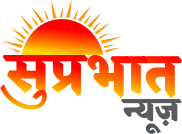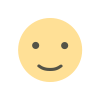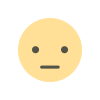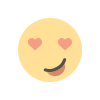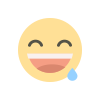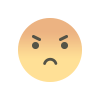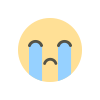दूरसंचार विधेयक को संसद में किया गया पेश, सैटकॉम स्पेक्ट्रम के लिए नहीं है कोई नीलामी
यदि टेलीकॉम कंपनियां पट्टे की अवधि से पहले अपना स्पेक्ट्रम सरेंडर करती हैं

दिल्ली : लोकसभा में पेश किया गया दूरसंचार विधेयक, 2023 का मसौदा सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी या सभी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क को संभालने, प्रबंधित करने या निलंबित करने की अनुमति देता है।
दूरसंचार विधेयक, 2023 का लक्ष्य 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलना है जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इस विधेयक को संसद में पेश किया जा चुका है।
इस विधेयक के बारे में बता दें कि ये स्पेक्ट्रम, लाइसेंसिंग और विवाद समाधान के आसपास प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक प्रक्रियाओं को सरल बनाने का भी प्रयास करता है। एक बड़ा बदलाव यह है कि सरकार विभिन्न सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग से प्राधिकरण की ओर बढ़ी है। यह प्रथा अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित है।
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई), इंडियन स्पेस एसोसिएशन (आईएसपीए), ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन जैसे उद्योग निकायों ने इन प्रावधानों का दिल से स्वागत किया। इन उद्योग निकायों का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा, दूरसंचार के विकास के बीच का संतुलन मिलेगा।
अपनी तरह के पहले विधेयक में प्रशासनिक मार्ग से उपग्रह संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन का रास्ता साफ हो गया है। ऐसा इन सेवाओं को अनुसूची 1 के अंतर्गत रखकर किया गया है,
जहां अब तक सिर्फ सरकारी और सुरक्षा संबंधी सेवाएं ही शामिल थीं। पहली बार निजी कंपनियां इस सूची में शामिल होंगी। इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद वनवेब, जियो सैटेलाइट, स्टारलिंक जैसी कंपनियों को किसी भी प्रकार की नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। इसके लिए मूल्य निर्धारण का काम ट्राई के साथ विचार कर तय किया जाएगा।
बता दें कि यह मुद्दा सबसे विवादास्पद था क्योंकि रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया जैसे दूरसंचार ऑपरेटर नीलामी के लिए कह रहे थे, जैसी तकनीकी कंपनियां प्रशासनिक आवंटन के पक्ष में थीं।
हालांकि इन सभी कंपनियों में भारती एयरटेल एकमात्र टेलीकॉम कंपनी थी जो नीलामी के पक्ष में नहीं थी। इसी तरह ओटीटी संचार ऐप्स को विनियमन के तहत लाने का अन्य प्रमुख विवादास्पद मुद्दा दूरसंचार कंपनियों के पक्ष में नहीं गया है।
इन ऐप्स पर किसी भी अतिरिक्त नियामक या लाइसेंसिंग ढांचे या शुल्क का बोझ नहीं डाला जाएगा। वे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लागू मौजूदा मानदंडों के तहत ही काम करते रहेंगे। हालाँकि, विधेयक सरकार को भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर ओटीटी को किसी भी प्रकार के विनियमन के तहत लाने के लिए अधिकृत करता है।
विधेयक में दूरसंचार ऑपरेटरों के दिवालियापन और उनके द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान में चूक से संबंधित दो विवादास्पद प्रावधानों को भी हटा दिया गया है।
विधेयक के पहले के मसौदे में DoT ने एक प्रावधान रखा था जिसमें कहा गया था कि किसी भी दूरसंचार सेवा प्रदाता के खिलाफ किसी भी दिवालिया कार्यवाही की स्थिति में, बाद वाले को सरकार को बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
आसा नहीं करने की स्थिति में सौंपा गया स्पेक्ट्रम रद्द कर दिया जाएगा, इस आदेश को भी वापस लिया गया है। इसे अब कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता में संशोधन करके अलग से संबोधित किया जाएगा।
पहले, सरकार वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए भी इच्छुक थी, जिसे अब विधेयक के तहत हटा दिया गया है ताकि भविष्य में कोई दुरुपयोग न हो।
विधेयक के तहत स्पेक्ट्रम सुधारों के हिस्से के रूप में, सरकार निर्धारित स्पेक्ट्रम के साझाकरण, व्यापार, पट्टे और आत्मसमर्पण की अनुमति दे सकती है, जो लागू शुल्क या शुल्क सहित नियमों और शर्तों के अधीन है।
हालाँकि, यदि टेलीकॉम कंपनियां पट्टे की अवधि से पहले अपना स्पेक्ट्रम सरेंडर करती हैं तो वे किसी भी रिफंड के लिए पात्र नहीं होंगे। विधेयक का उद्देश्य अप्रिय कॉलों और अन्य मुद्दों के खिलाफ शिकायतों को संभालने के लिए
एक शिकायत निवारण तंत्र और ऑनलाइन विवाद समाधान प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के संबंध में, विधेयक सरकार को सेवाओं को निलंबित करने या दूरसंचार नेटवर्क का अधिग्रहण करने की शक्ति देता है।
धोखाधड़ी वाले सिम कार्डों को रोकने के लिए, विधेयक में उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले दूरसंचार कंपनियों द्वारा बायोमेट्रिक पहचान को अनिवार्य करने का प्रावधान शामिल है।
विधेयक में उन विवादास्पद प्रावधानों को भी हटा दिया गया है जो पहले संस्करण में ट्राई की शक्तियों को कम करने का संकेत देते थे। इसके अलावा, इसमें यह प्रावधान भी किया गया कि प्रासंगिक योग्यताएं निर्धारित करते हुए ट्राई के अध्यक्ष को अब निजी क्षेत्र से भी नियुक्त किया जा सकता है।